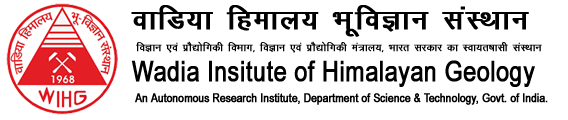संस्थापक
 प्रो. डी.एन. वाडिया प्रोफेसर दाराशॉ नौशेरवान वाडिया का जन्म 23 अक्टूबर, 1883 को सूरत में हुआ था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज बनाने वाले एक सम्मानित परिवार से थे, जो सूरत गुजरात, भारत में और उसके आसपास बस गए थे।
प्रो. डी.एन. वाडिया प्रोफेसर दाराशॉ नौशेरवान वाडिया का जन्म 23 अक्टूबर, 1883 को सूरत में हुआ था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज बनाने वाले एक सम्मानित परिवार से थे, जो सूरत गुजरात, भारत में और उसके आसपास बस गए थे।
दारा, जैसा कि परिवार उन्हें प्यार से बुलाता था, को अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए सूरत भेजा गया था। उन्होंने ये साल अपनी नानी की सख्त देखभाल और अनुशासन में बिताए। उन्होंने पहले निजी गुजरात स्कूल में पढ़ाई की और फिर जे.जे. इंग्लिश स्कूल में दाखिला लिया।
12 साल की उम्र में दारा ने बड़ौदा हाई स्कूल में दाखिला लिया। वे अपने सबसे बड़े भाई, स्वर्गीय एम.एन. वाडिया, जो बड़ौदा राज्य के एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् थे, से बहुत प्रभावित थे और उनकी निजी देखरेख में उनमें प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम, ज्ञान के प्रति समर्पण और सीखने के प्रति उत्साह विकसित हुआ।
1905 में प्रो. वाडिया ने बड़ौदा कॉलेज से प्राकृतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के विषयों के साथ कला और विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। भूविज्ञान में उनकी रुचि, जो अब तक भारत में कम पढ़ाया जाने वाला विषय था, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अदारजी एम. मसानी द्वारा जगाई गई थी। उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री के लिए भूविज्ञान को एक विषय के रूप में पेश किया, भले ही उस समय बड़ौदा कॉलेज में भूविज्ञान में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। उन्होंने ज्यादातर स्व-अध्ययन और व्यक्तिगत छात्रवृत्ति के माध्यम से क्रेडिट के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वाडिया ने बाद में बड़ौदा कॉलेज में कुछ समय के लिए व्याख्याता के रूप में भी काम किया।
वाडिया को 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जम्मू में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। जम्मू ने उनके भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया और उनकी योग्यता और क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें शुरू से ही भूविज्ञान विभाग को व्यवस्थित करने का कार्य सौंपा गया।
उन्होंने 1921 तक कॉलेज में अध्यापन जारी रखा, उसके बाद उन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक का पद स्वीकार कर लिया। जम्मू में अपने कार्यकाल के दौरान, प्रो. वाडिया ने 1907 से 1920 तक अपनी छुट्टियों के अधिकांश वर्षों को भूवैज्ञानिक क्षेत्र के कामों में लगाया और इस दौरान उन्होंने हिमालय के बारे में कुछ नए विचारों को गढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री और साक्ष्य एकत्र किए। 1919 में उन्होंने अपनी पुस्तक जियोलॉजी ऑफ इंडिया (मैकमिलन, लंदन) प्रकाशित की।
वाडियास को 38 वर्ष की अपेक्षाकृत अधिक आयु में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे उन्हें उत्तर-पश्चिमी हिमालय की स्ट्रेटीग्राफी और टेक्टोनिक्स पर भूवैज्ञानिक शोध करने के लिए पर्याप्त अवसर मिले। उत्तर-पश्चिमी पंजाब, वजीरस्तान, हजारा और कश्मीर में गहन और विस्तृत कार्य के साथ, वे न केवल इस जटिल क्षेत्र की संरचना की व्याख्या करने में सक्षम थे, बल्कि पूरे देश में भूवैज्ञानिक सोच को भी प्रभावित कर सके।
वे 1938 तक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ थे। सर्वेक्षण के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 1926-1927 में ब्रिटिश संग्रहालय में अपनी अध्ययन छुट्टी बिताई, जहाँ उन्होंने पोटवार और कश्मीर से एकत्र कशेरुकी जीवाश्मों पर काम किया। उन्होंने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में भूवैज्ञानिक संस्थानों का भी दौरा किया और जिनेवा विश्वविद्यालय में एपलाइन भूविज्ञान में एक कोर्स में भाग लिया। उत्तरपश्चिमी हिमालय के सिंटैक्सिस पर उनके पेपर, नंगा पर्वत के एक महत्वपूर्ण बिंदु के चारों ओर पूरे हिमालयी बेल्ट के तीव्र धनुषाकार घुटने के मोड़ ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से ख्याति दिलाई। 1937 में, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस, मास्को के अनुरोध पर उन्होंने उत्तर भारतीय वनभूमि के साथ हिमालय के टेक्टोनिक संबंधों पर अपना प्रसिद्ध पेपर दिया।
वाडिया 1938 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से सेवानिवृत्त हुए, जब उन्हें सीलोन (अब श्रीलंका में) में सरकारी खनिज विज्ञानी के पद की पेशकश की गई। उन्होंने इस द्वीप के भूविज्ञान का गहन अध्ययन करने में लगभग छह साल बिताए, जिसे वे भारतीय प्रायद्वीप का सुंदर पेंडेंट मानते थे।
डॉ. वाडिया को 1944 में भारत सरकार का भूवैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए खनिज नीति की शुरुआत की और उसे तैयार किया।
भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग ने रेडियोधर्मी कच्चे माल के घरेलू संसाधनों की खोज के लिए 1949 में अपना परमाणु खनिज प्रभाग स्थापित किया और डॉ. वाडिया इसके पहले निदेशक बने। 15 जून, 1969 को अपनी मृत्यु तक वे इस इकाई के प्रमुख बने रहे।
हिमालय के अध्ययन के प्रति वाडिया का प्रेम और समर्पण असीम था। उनकी पहल और प्रयासों के कारण ही 1968 में हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना हुई। उनकी याद में संस्थान का नाम बदलकर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया। हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और गोवा के पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना करवाने में भी वे ही जिम्मेदार थे।
उन्हें 1934 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का बैक पुरस्कार और 1943 में लंदन जियोलॉजिकल सोसाइटी का रॉयल मेडल प्राप्त हुआ।
इसके बाद वे 1945-46 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान (जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहा जाता है) के अध्यक्ष, भारतीय खनन भूवैज्ञानिक और धातुकर्म संस्थान (1950), भारतीय भूवैज्ञानिक खनन और धातुकर्म सोसायटी, भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी, भारतीय इंजीनियरिंग भूविज्ञान सोसायटी, भारतीय भूगोलवेत्ता संघ और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सोसायटी के मानद संवाददाता रहे।
इस अवधि के दौरान उन्होंने सीएसआईआर सहित कई वैज्ञानिक संस्थानों की शोध सलाहकार समितियों का नेतृत्व भी किया। 1957 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया, जो अब तक किसी अन्य भारतीय भूविज्ञानी को नहीं मिला। उनके करियर का सबसे बड़ा सम्मान भूविज्ञान में प्रोफेसर के रूप में मिला। उन्होंने दिसंबर 1964 में नई दिल्ली में आयोजित XXII अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की अध्यक्षता की।
भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉ. वाडिया ने लगभग सौ मौलिक शोध पत्र, विभिन्न विषयों पर मोनोग्राफ और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभिलेख और स्मृतियाँ लिखीं।